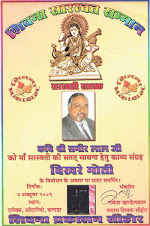(पद्दमश्री स्व. पं भवानी प्रसाद तिवारी के सौवें जन्म दिवस पर विशेष)
दर्द उनका, अश्क बनकर, वाँ गिरा वो काँ मिला ?
ढूंढते तो सब रहे पर, आख़िर हमको याँ मिला !
अपने इस शेर को हम, इस लेख के उनवान की नज़्र कर रहे हैं क्योंकि, इस शीर्षक और इसके तले कुछ लिखने का मौक़ा मिलने से बेहतर आशीर्वाद हमारे लिए और हो भी क्या सकता है भला ? अहा ! ‘उस्ताद के उस्ताद पर उस्ताद का नज़रिया’ ! क्या कहना ! और इसके लिए हमारा इंतिख़ाब भी काफ़ी सोच समझ कर किया गया लगता है। भई, वजह भी तो ज़ाहिर है। अरे, जब तक हम ‘काव्य’ को समझ पाने की वय पाते, तब तक ‘रसज्ञ’ तो दुनिया को अपनी ‘माटी की गागरिया’ में ‘रस भरी सागरिया’ सौंप कर महाप्रयाण कर चुके थे।
नाना प्रकार और नाना
और नहीं तो क्या ? अब दुनिया जानती रही होगी उनको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कविवर, गीतकार, पत्रकार, ‘काव्य रसज्ञ’, पूर्व महापौर, पूर्व राज्य सभा सांसद, नगर प्रहरी, पद्मश्री पंडित भवानी प्रसाद तिवारी, पंडित जी, पापाजी जैसे नाना प्रकार के नामों से और रूपों में। मगर हम तो बस इतना ही जानते थे कि, आप हमारे और नानाओं (किशोर कुटी वाले डॉ. सी. के. तिवारी एवं बंधु) जैसे ही एक ‘नानाजी’ थे। कभी-कभी जब हमारे घरों की गौवें इनके बंगले-बाड़ी में घुस जाती थीं और हम अपनी छोटी सी साइकिल पर लठिया-गिरमा लिए उन्हें लिवाने इनके कने पहुँच जावें, तो आप बनावटी गुस्सा दिखलाते हुए अपनी जादुई छड़ी से गौवों को बड़े प्यार से हमारी तरफ़ हकालते हुए कहें कि, “ए डाक्टर के नाती, अबकी दफ़े तेरी गैया आई, तो हम सब दूध यहीं दुह लेंगे, फिर तू क्या पिएगा बोल”? और फिर ठहाका मारकर हँस देवें और हम भाग छूटें। या कभी-कभी इतवार को जब हम दादा रघुनाथ नाई की दूकान पर कुर्सी के हत्थों पर रखे पटिये पर बैठे बाल कटाते हों और आप कहीं पहुँच जावें, तो नाई की कैंची की कच-कच-कच-कच के बीच कहें-“हाँ भाई रघुनाथ, जरा इस छोटू के थोड़े थोड़े कान भी काट लईयो, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, यार”। और जब हम जवाब में “आँ sss” करें तो कहें कि, “चल अच्छा, कान नहीं तेरी गैया की दुम काट लेंगे बस, हा हा”। तब भी वही हो याने कि “आँ sss” । इसके आगे के भवानी को हम क्या जानते थे तब भला ? हाँ, जिन्होंने बतलाया वो थे, हमारे शहज़ादे मियाँ सारंग के “माती की गागलिया वाले नानाजी”, याने......
वाह ! भाई लुकमान
सन् १९७२-७५ का ज़माना रहा होगा शायद। हम भी क्या, तब बालिश्त भर के ही रहे होंगे। धुरेड़ी के दिन, रंग-पिचकारियों के संग, साथियों की हुड़दंग से निपट-थक-सोकर के थोड़ी शाम-थोड़ी रात को जागे ही थे कि कोई बाहर बुलौवा दे गया। “कक्काजी, पंडितजी के इते लुकमान की कब्बाली है, सुनबे आ जईयो।” सो भोजनोपरांत नानाओं (तिवारी बंधु) और मामाओं के संग अपन भी लटक लिए।
अहा! क्या ढोलक-बाजा-गाना और तालियाँ सज रहीं थीं वहाँ! वाह वाह! अब हमें वह काव्य-गीत-क़व्वाली तो क्या ही समझ आती पर हरेक रचना के बाद, जब भवानी नाना अपने माथे पर पड़ी बालों की लटों को गर्दन के झटके से पीछे करते हुए दाद दें कि, “वाह भाई लुकमान,” और चचा हौले से मुस्करा कर दाद स्वीकार करें तो न जाने क्यों हमको भी बड़ा मज़ा आता था। अदब को बासलीक़ा पेश करने, उसकी तारीफ़ करने और पाने का वैसा अंदाज़, हमने तमाम उम्र कभी भी और कहीं भी नहीं देखा।
आला दर्जे के साहित्य और रूहानी सूफ़ियाना संगीत के रंगों से सराबोर, उस सुहानी महफ़िल की एक अमिट याद, हमारे दिल में बस कर रह गई। चचा लुक़्मान की कर्णप्रिय आवाज़, ये बोल “माटी की गागरिया”, “हाल गुज़रगाहे वफ़ा का देखा” और गुलशेर मियाँ की शानदार ढोलक की वो गमक। बस, इसके आगे बहुत लम्बा अरसा गुज़र गया।
बिटिया ने मिलाया चचा लुक़्मान से
सन् १९९५ में जब हमारी बिटिया सिद्धीबाला के बारसे का आयोजन होना था तो न जाने क्यों और कहाँ से ज़ेहन में ‘माटी की गागरिया’ की भूली बिसरी याद आ गई और चचा लुक़्मान को सुनने की तड़प जाग उठी। अम्माजी (श्रीमती नंदिनी दुबे, एड्वोकेट) बोलीं, “तुम्हारी पहली सालगिरह पर बहुत बड़ी महफ़िल हुई थी उनकी। तब शहर भर के गणमान्य और प्रबुद्ध नागरिक आए थे। तमाम मैदान भर गया था और सामने की सड़क तक जाम हो गई थी। क्या पता अब वो हैं भी के नहीं, बहुत बरसों से उनके विषय में सुना भी तो नहीं।”
ख़ैर, जब दिल ना माना तो मोहल्ले-मोहल्ले बगैर गूगल के ही, सर्च करते हुए गोहलपुर की अलिफ़-बे मस्जिद के पीछे से खोज ही लाए हम चचा लुक़्मान को। अहा! क्या महफ़िल हुई फिर ! लाजवाब !
बरसों की प्यास को स्वाति की बूँद थी वह, वह महफ़िल।
पंडितजी और चचा लुक़्मान की निस्बत
हफ़्ते भर बाद ही चचा न जाने क्या सोचकर हमारे पास आए और कहा - “अपनी तो चला-चली की बेला है, ले लो जो कुछ लेना हो भाई।” हम तो तत्काल विधिवत उनके शागिर्द बन गए। सीखने सिखाने के दौर में जब चचा से बातें हों और वे यादों में खो जाएँ, तो पंडितजी का नाम आते ही उनकी आँखें नम हो जाती थीं। हमेशा कहते थे, “पंडितजी चले गए, बस महफ़िल उठ गई यार।” चचा के दिल से पंडितजी के लिए बस कुछ इसी तरह निकलता था-
गीत अधूरे, तुम बिन मेरे, साज़ों में कोई तार नहीं
बिखरी हैं रचनाएँ सारी, शब्दों में कोई सार नहीं
“दौरे-क़ाबे की ज़ियारत तो फ़क़त हीला है
जुस्तजू तेरी लिए फिरती है घर घर मुझको।” --- जलील
कुछ देर ख़ामोश रहकर हमने उनसे कहा कि चचा हमें कुछ और बतलाइए ना पंडितजी के बारे में। उनकी नज़रें कह उठीं-
चलो मिलाते हैं तुमको उनसे, यहीं कहीं है पड़ाव उनका
औ’ जब मिलोगे तो देख लेना, है हमसे कितना जुड़ाव उनका
--- ‘बवाल’
पंडित भवानी की कहानी - चचा लुक़्मान की ज़ुबानी
चचा ने आगे फ़रमाया- “सन् ५२ के आसपास की बात है, गनेशों के दिन थे। जी! गढ़ा में एक वक़ील साहब हुआ करते थे, वहाब। उन्होंने मुझसे कहा- चलते हो पंडितजी कने? मैंने कहा- मैं तो नहीं जानता कौन पंडितजी हैं? कहने लगे- मेयर हैं यार चले चलो। मैंने कहा- क्या करेंगे हम वहाँ जाके यार? कहने लगे- नहीं नहीं चलो तो, बड़े शौकीन लोग हैं। मैंने कहा हमारे जैसे शौकीन हों तो ठीक है वरना शास्त्रीय संगीत तो मैं जानता नहीं। ख़ैर, जब पंडितजी के यहाँ पहली ग़ज़ल, ‘तू बेहिजाब है आईना तुझको तकता है, संभल संभल ये सितम कौन देख सकता है’ गाई, तो बहुत पसंद की गई। याने हद से ज़्यादा पसंद की गई। सुरेन्द्रनाथ शुक्ला जी वगैरह बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। यहाँ ग़ज़ल ख़त्म हुई और पंडितजी जी, जो कहीं बाहर गए हुए थे, ठीक तभी आए। कहा- नहीं नहीं भाई, फिर से शुरू हो। फिर से ग़ज़ल हुई। मैंने उन्हें देखा। बड़े पुरख़ुलूस शख़्स नज़र आए। क्या कहना ! पंडितजी ने सुनने के बाद कहा- भाई, अब इसके ऊपर ही चलना है, नीचे नहीं जाना है। उस हौसले ने मुझे काफ़ी बुलंद कर दिया।
इतने लोगों से मिला जीवन में मैं बवाल। (हमारा यह तख़ल्लुस चचा लुक़्मान का ही दिया हुआ है) सब एक से बढ़कर एक अदीब। मगर पंडितजी पंडितजी ही थे। ‘एक सम्पूर्ण जाग्रत साहित्य, ओज में मौन का शिष्ट मिश्रण। स्नेह में भी साधना, ऋण में उऋण, आरोह में समारोह, चैन में नैन और नैन में बैन, प्यार में ज्वार और ज्वार में बयार, हर वय में लय, चँचलता में सुधि, अनगिनगुन वैविध्य का कोषागार, प्राण पूजन की निरापद धारा, निज़ाम का निबाह, तम्कीन का तर्जुमा, अदबआरा, रम्ज़ आगाह और दल्क़पोश शाह।’ क्या क्या नहीं किया यार उन्होंने हमारे लिए। ज़िंदगी तेर कर दी। लाईब्रेरी की नौकरी लगवाई, जीवन भर के लिए जुगाड़ कर गए। नामालूम कितने प्रोग्राम करवाए। उषा-भार्गव कांड के समय जान हथेली पर रखकर हमारी ख़ैर ख़बर लेते रहे। हमारे टूटे हुए मन को उन्होंने हमेशा संभाला वरना अपनी बिसात क्या। पड़े रहते एक कोने में कहीं।”
चलते चलते
हम दोनों की डबडबाई आँखें एक दूजे से बस इतना ही कह पाईं फिर-
तुमने मेरी आम नज़र से, ख़ास भला क्या क्या देखा ?
अँधेरे की थाह से उभरा, बिसरा उजियारा देखा !
--- ‘बवाल’ हिंदवी